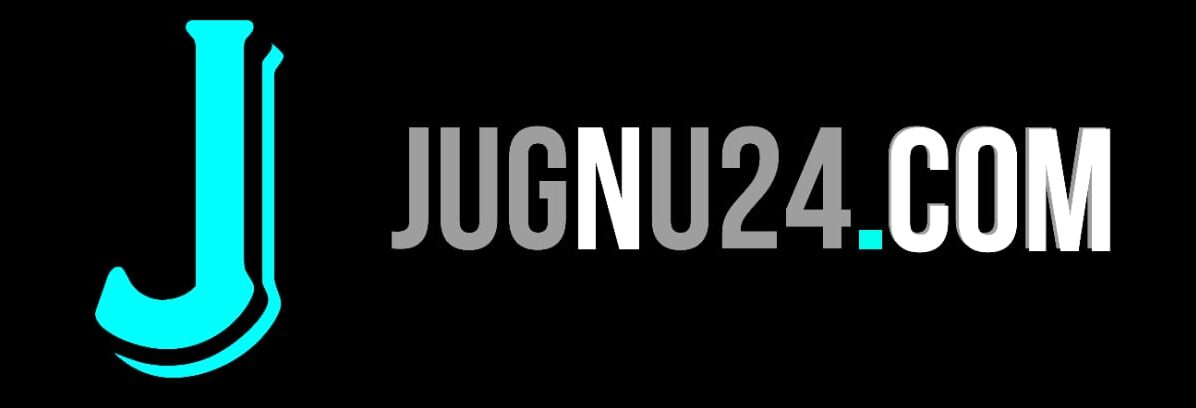आज़म ख़ान साहब और उनके बेटे अब्दुल्लाह साहब की जेल की सलाखों के पीछे की ख़ामोशी, दरअसल एक पूरी क़ौम के दर्द और बेचैनी की आवाज़ बन गई है
आज आज़म ख़ान साहब और उनके बेटे अब्दुल्लाह साहब की जेल की सलाखों के पीछे की ख़ामोशी, दरअसल एक पूरी क़ौम के दर्द और बेचैनी की आवाज़ बन गई है ऐसा लगता है जैसे उनकी आँखों के ज़रिये आज हिंदुस्तान के मुसलमान अपने हालात, अपने डर और अपने सवाल इस मुल्क से पूछ रहे हों

जेल की टूटी हुई सीढ़ियों पर बैठा हुआ एक बुज़ुर्ग नेता
ज़रा तसव्वुर कीजिए एक पुरानी जर्जर जेल की टूटी हुई सीढ़ियों पर बैठा हुआ एक बुज़ुर्ग नेता जिसे कभी “मुसलमानों की आवाज़” कहा जाता था हालांकि आज भी वही आवाज़ हैं वही हमदर्द हैं गरीबों बेबसों ओर मुस्लिमों के
उनकी जगह इस दौर में कोई नहीं ले सकता उसके साथ उसका जवान बेटा, अब्दुल्लाह आज़म ख़ान जिसकी आँखों में कभी नई सियासत और नए हिंदुस्तान के सपने थे आज तारीख़ें, मुक़दमे और सज़ाओं की गिनती करते‑करते थक चुका सा गए हैं
लेकिन अलहम्दुलिल्लाह हारे नहीं हैं ।
चारों तरफ़ ऊँची दीवारें, जंग लगी सलाखें, और दूर खड़ी पुलिस की वर्दियाँ उन्हें बार‑बार याद दिलाती हैं कि क़ानून की लड़ाई अक्सर कमज़ोर पर ज़्यादा सख़्त पड़ जाती है
दोनों के दिल में एक ही सवाल बार‑बार उठता है क्या हमारा कसूर सिर्फ़ ये है कि हम मुसलमान हैं और हक़ की बात करने वाले सियासी लोग हैं
क़ुर्बानियाँ:
आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों का ख़ून भी इसी मिट्टी ने सोखा था, उनके भी बेटे उसी तिरंगे के लिए फाँसियों पर चढ़े थे। उस वक़्त किसी ने उनसे नहीं पूछा था कि उनका मज़हब क्या है सिर्फ़ ये देखा था कि वो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दे रहे हैं l
लेकिन आज हाल यह है कि रिपोर्टें दिखाती हैं कि दंगों नफ़रती तशद्दुद, झूठे मुक़दमों और नफ़रत भरी राजनीति का सबसे भारी बोझ अक्सर #मुसलमानों पर ही आकर गिरता है। जब किसी शहर में सिर्फ़ एक ही तबक़े के घरों पर बुलडोज़र चलता है, एक ही समुदाय के नौजवाँ को बार‑बार “संदिग्ध” कह दिया जाता है, तो दिल पूछता है “क्या हमारी सारी क़ुर्बानियाँ सिर्फ़ तारीख़ की किताबों तक सीमित होकर रह गईं
नफ़रत के बीज
नफ़रत के बीज कुछ सियासी चेहरों, कुछ टीवी बहसों और कुछ ज़हरीले नारों ने धीरे‑धीरे समाज में ऐसा बीज बोया कि आम ज़िंदगी भी शक‑ओ‑शुब्हे से भरती चली गई । अब किसी मुसलमान नौजवाँ को सबसे पहले ये डर लगता है कि उसका नाम, उसकी दाढ़ी, उसकी टोपी या उसकी पहचान कहीं उसके लिए मुसीबत न बन जाए।
थाने से अदालत तक और सोशल मीडिया से चाय की दुकानों तक, जब एक ही तरफ़ का बयान ज़्यादा तेज़ी से गूंजता है, तो दूसरी तरफ़ के लोग अपने को अकेला और घिरा हुआ महसूस करने लगते हैं ।
आज़म ख़ान साहब जैसे बुज़ुर्ग नेता जब अपने ऊपर दर्ज दर्जनों मुक़दमों और सज़ाओं को देखते हैं तो उन्हें अक्सर लगता होगा कि ये सज़ा सिर्फ़ काग़ज़ी जुर्म की नहीं बल्कि उनके मज़हब उनकी ज़ुबान और उनकी सियासी बैकग्राउंड की भी है।
गांधी जी का सपना, टुकड़ों में बँटी तस्वीर
महात्मा गांधी ने जिस हिंदुस्तान का सपना देखा था उसमें #मंदिर की घंटी और मस्जिद की अज़ान एक ही आसमान के नीचे बराबर की इज़्ज़त के साथ गूँजती थी। उनका मानना था कि हिंदू‑मुस्लिम‑सिख‑ईसाई सब मिलकर ही इस मुल्क की रूह बनते हैं, और अगर किसी एक को कमज़ोर किया जाए तो पूरा मुल्क कमज़ोर हो जाएगा।
आज हाल यह है कि गांधी जी की तस्वीर तो हर सरकारी दफ़्तर की दीवार पर टंगी रहती है, लेकिन उनके सपने का रंग कई जगहों पर फीका पड़ता नज़र आता है। जो भारत “सभी धर्मों के लिए बराबर” कहलाता था, वहीं अब कई लोग अपने मज़हब की वजह से खुद को कटघरे में खड़ा महसूस करते हैं ।
अँधेरे में उम्मीद का एक छोटा‑सा चिराग़
फिर भी इस घने अँधेरे में उम्मीद का एक छोटा‑सा चिराग़ जलता हुआ दिखता है: हर शहर, हर गाँव में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो #ज़ुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, चाहे वो ज़ुल्म किसी भी धर्म के इंसान पर हो l जब कोई हिंदू पड़ोसी अपने मुसलमान दोस्त के लिए अदालत में गवाही देता है, या कोई मुसलमान किसी दूसरे धर्म के मज़लूम के लिए आवाज़ उठाता है, तब गांधी के सपने का एक टुकड़ा फिर से ज़िंदा महसूस होता है ।
आज़म ख़ान साहब और उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म ख़ान साहब की क़ैद एक दिन तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन असली सवाल यह है कि तब तक हम नफ़रत के इस मौसम को कितना बढ़ने देंगे । ज़रूरत इस बात की है कि हम मज़हब के नाम पर दीवारें नहीं बल्कि इंसानियत के नाम पर पुल बनाएं, जहाँ किसी को अपने नाम, अपने धर्म या अपनी पहचान का सबूत देकर जीना न पड़े।